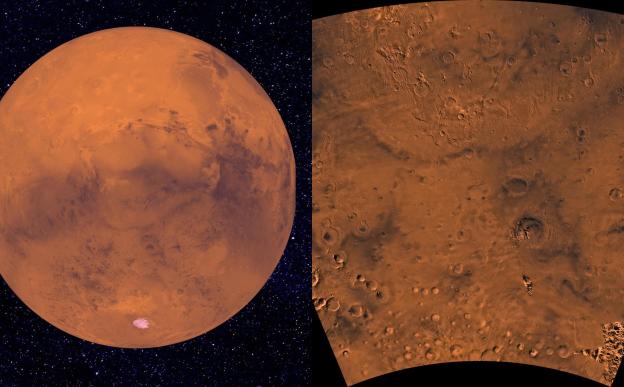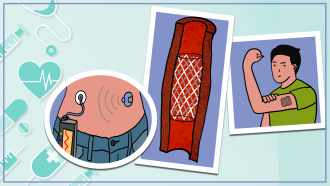कृषि क्षेत्र का आकार में बड़ा होना ही सदैव अधिक लाभदायक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। 1960 से हुए अध्ययन बताते हैं कि प्रति एकड़ उपज की दृष्टि से, बड़े खेतों की तुलना में छोटे खेत अधिक ऊपजाऊ होते हैं। औद्योगिक नियमों के विपरीत कृषि क्षेत्रों का यह चलन वैज्ञानिकों एवं नीति निर्माताओं को विस्मित करने वाला है। वैश्विक स्तर पर कृषि भूमि के प्रायः 90 % भाग पर छोटे एवं पारिवारिक खेतों का वर्चस्व है एवं इस चलन ने दशकों से कृषि नीतियों एवं निवेश को प्रभावित किया हुआ है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई (आईआईटी मुंबई) एवं हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने एक नूतन अध्ययन में कृषि क्षेत्र के इस विस्मय को एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। अध्ययन बताता है कि खेत के आकार एवं उत्पादकता के मध्य स्थित यह प्रतिलोम संबंध, भारत के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कभी भी इतना स्पष्ट नहीं रहा। कृषि संबंधी संकटों के चलते आगे के वर्षों (2009 से 2014) में इन क्षेत्रों में स्थित छोटे आकार के खेतों से होने वाला उत्पादन लाभ सीमित हो गया। अध्ययन महत्वपूर्ण नीतिगत प्रभावों को सामने ला सकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या का प्रायः आधा भाग, दो हेक्टेयर से भी कम भूमि वाले अल्पभूधारक किसान हैं।
“विकासशील राष्ट्रों में खेतों के आकार एवं उनसे प्राप्त उपज के मध्य का यह संबंध दशकों से चर्चा का विषय रहा है। हमारी खोज का निष्कर्ष यह है कि खाद्य सुरक्षा एवं ग्राम्य स्थिरता में छोटे किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु एकल उपज (मोनोक्रॉप) एवं उच्च निवेश राशि के कारण वे निरंतर असुरक्षित होते जा रहे हैं। हमारा मानना है कि इस समस्या के समाधान हेतु उचित तकनीक, सरल ऋण एवं विश्वसनीय सेवाओं को छोटे किसानों की पहुँच में लाकर हमें उनके सामर्थ्य को बढ़ाना होगा,” इस अध्ययन के सहलेखक प्रा. सार्थक गौरव का कहना है, जो आईआईटी मुंबई के शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्राध्यापक हैं।
इस अध्ययन हेतु शोधकर्ताओं ने इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दि सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) से प्राप्त डेटासेट का उपयोग किया जो कि ग्राम स्तरीय अध्ययन पर आधारित एवं 1975 से 2014 तक के चार दशकों तक विस्तारित था। यह विस्तृत डेटाबेस अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किये जाने वाले सर्वाधिक दीर्घकालिक कृषि अध्ययनों में से एक के रूप में मान्य है, क्योंकि यह कई दशकों तक पारिवारिक कृषि का अध्ययन करता है। भारतीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय ग्रामीण क्षेत्रों के इतने समृद्ध डेटाबेस की उपलब्धि के उपरांत भी शोधकर्ताओं ने पाया कि इसमें दीर्घकालिक परिवर्तनों के आकलनों का अभाव है, जो खेतों के आकार एवं उत्पादकता के मध्य संबंध को दर्शाता है।
भारत में समुद्री तट से दूर स्थित अधिकांश प्रायद्वीपीय भाग अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जहाँ कृषि मुख्यतः अनिश्चित वर्षा पर निर्भर होती है। यहाँ वर्षा औसत रूप से 400 से 800 मिलीमीटर वार्षिक दर से होती है। यद्यपि यह भाग अनेकों राज्यों को स्पर्श करता है, ICRISAT डेटा मुख्यतः तीन प्रतिनिधि क्षेत्रों को दर्शाता है - अकोला, सोलापुर एवं महबूबनगर। यह क्षेत्र हरित क्रांति के प्रारंभिक लाभों से वंचित है। शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र की अनूठी कृषि-पारिस्थितिकी एवं संस्थागत स्थितियाँ, कृषि में विलंबित किंतु महत्वपूर्ण परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पादकता में कैसे परिवर्तन हुए, इसके अध्ययन के लिए इसे एक आदर्श क्षेत्र बनाते हैं।
यह नवीन शोध भारत के अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खेत के आकार एवं उत्पादकता पर किया गया संभवतः प्रथम अध्ययन है। शोधकर्ताओं को विशाल ICRISAT डेटासेट का विश्लेषण करने में अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चूंकि डेटा विभिन्न चरणों में एकत्र किया गया था, उन्हें सर्वेक्षण की विभिन्न लहरों में से घरेलू एवं कृषि से संबंधित डेटा को आपस में जोड़ने में महीनों का समय लग गया। इस दीर्घ समयावधि को ध्यान में लेते हुए डेटा में उत्पन्न हुई विसंगतियों के कारण उन्हें भूखंडों से घरेलू स्तर के विश्लेषण में स्थानांतरण सहित अपनी पद्धति में संशोधन भी करना पड़ा। अध्ययन में डेटाबेस की कमियों को दूर करने हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग के ग्रिडेड डेटा (चौकट में विभाजित पद्धति का डेटा) जैसे बाह्य स्रोतों का भी उपयोग किया गया।
शोधकर्ताओं ने पाया कि विशेषकर पूर्व के वर्षों (1975 - 1984) में छोटे आकार के खेतों की उत्पादकता अधिक थी। पूर्व के अध्ययनों में खेत के आकार एवं उत्पादकता के मध्य स्थित इस प्रतिलोम संबंध पर बहुत से स्पष्टीकरण दिये गए हैं। सर्वाधिक प्रचलित स्पष्टीकरण के अनुसार छोटे आकार के खेतों वाले किसान बड़े भूमिधारकों की तुलना में अत्यधिक पारिवारिक श्रम कर लेते हैं, उनका ध्यान खेत पर अधिक केंद्रित होता है एवं वे प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। यद्यपि नवीन अध्ययन से सिद्ध होता है कि उन पूर्व के वर्षों में भी छोटे आकार के खेतों की उत्पादकता उतनी अधिक नहीं थी जितनी कि पूर्व के अध्ययनों में मानी गई है।
शोधदल ने जब प्रत्येक खेत में उपयोग किए जाने वाले श्रम एवं उर्वरक की मात्रा पर ध्यान दिया, तब छोटे आकार के खेतों में अधिक उत्पादकता लाभ सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन पाया गया।
“श्रम एवं श्रम-रहित निवेश जैसे कि बीज, उर्वरक तथा यंत्र सामग्री, दोनों का भूमि उत्पादकता के साथ दृढ़ एवं सकारात्मक संबंध था। इससे ज्ञात होता है कि केवल भूमि का आकार महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उस खेत का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से किया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है,” प्रा. गौरव बताते हैं।
किन्तु इसमें एक समस्या देखी गई। छोटे खेतों में किया गया गहन निवेश भले ही सकल उत्पादकता को बढ़ा दे किंतु आवश्यक नहीं कि यह लाभकारी होगा। इस प्रकार छोटे भूमिधारकों ने अपने प्रयासों के माध्यम से प्रति एकड़ उपज में वृद्धि तो देखी किंतु यह संभवतः प्रति एकड़ लाभ में वृद्धि नहीं थी । इसके अतिरिक्त, विविध प्रकार की उपज लगाना छोटे किसानों के लिए बहुधा मौसम एवं बाजार की अनिश्चितता के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। किंतु अध्ययन बताता है कि ऐसा करना उत्पादकता एवं तकनीकी दक्षता दोनों को कम करता है। इस प्रकार इस अध्ययन के निष्कर्ष छोटा खेत एवं अधिक उत्पादकता जैसे प्रतिलोम संबंध होने की दीर्घकालिक धारणा को चुनौती देते हैं, एवं यह भी स्पष्ट करते हैं कि छोटे किसान वित्तीय रूप से संघर्षरत क्यों होते हैं।
इस अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि आगे के वर्षों में छोटा खेत और अधिक उत्पादकता का यह प्रतिलोम संबंध क्षीण तो हुआ किंतु व्यापक यंत्रीकरण के उपरांत भी यह पूर्ण रूप से नहीं पलट सका।
“हमें विश्वास था कि बढ़ते हुए कृषि यंत्रीकरण एवं बाजारों तक बेहतर पहुँच के साथ यह प्रतिलोम संबंध आने वाले समय में पलट कर सकारात्मक हो जाएगा। किंतु 2014 के आने तक भी यह किंचित मात्र ही सकारात्मक दिखा एवं पूर्ण रूप से नहीं पलट सका। इस संबंध का दीर्घकाल टिके रहना हमें महत्वपूर्ण संकेत देता है कि अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन कितना असमान एवं मंद हो सकता है,” प्रा. गौरव स्पष्ट करते हैं।
अध्ययन के निष्कर्ष खाद्य सुरक्षा, दरिद्रता उन्मूलन, स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी), कृषि नीतियाँ एवं कृषि क्षेत्रों में भूमि सुधार जैसे विभिन्न दूरगामी प्रभावों को इंगित करते हैं। विभिन्न नीतिगत दृष्टियों में से, प्रा. गौरव का प्राथमिक मत है कि छोटे किसानों की सामूहिक क्षमता में संशोधन होना चाहिए ताकि वे बाजारों एवं निवेश तक सरलता से पहुंच सकें। “हमने बहुत सी ऐसी चुनौतियों का निरीक्षण किया जो न केवल खेत के आकार से संबंधित थी अपितु बाजार आदान-प्रदान, आवश्यक संसाधनों एवं ज्ञान तथा आधारभूत सुविधाओं तक पहुँच के अभाव को भी व्यक्त करती थी। छोटे किसानों को सामूहिक दल या उत्पादक दलों में संगठित करने से उन्हें संसाधनों को एकत्रित करने, कृषि-पर्यावरणीय पद्धतियों से जुड़ने एवं उत्तम मूल्यों पर मोल-तोल करने में सहायता मिल सकती है,” प्रा. गौरव स्पष्ट करते हैं।
किसानों से प्राप्त डेटा के स्वयं सूचित होने से लेकर एक विशेष कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पर सीमित दृष्टि तक इस अध्ययन की अपनी कुछ सीमाएं हैं। यद्यपि खोज बताती है कि खेत का आकार एवं उत्पादकता का संबंध जटिल है, संदर्भ निर्भर है एवं पूर्व मान्य धारणा की तुलना में दुर्बल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि छोटे किसानों का प्रभाव घट रहा है अपितु यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि परिस्थितियों से अनुकूलन हेतु उन्हें समर्थन की आवश्यकता है। छोटे खेतों से होने वाले लाभों जैसे कि रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने के साथ ही उनकी आर्थिक सक्षमता में वृद्धि करना असली चुनौती है।