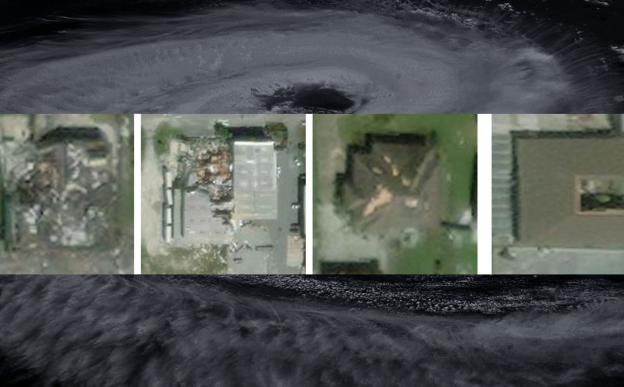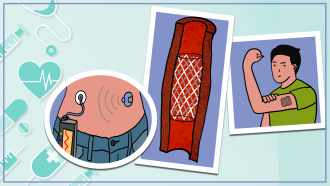जल हो या निधि, दोनों का ही कुशल प्रबंधन आवश्यक है। बैंक में निधि के सीमित होने पर लोग इसे सावधानी पूर्वक व्यय करते हैं। उसी प्रकार सूखा प्रवण क्षेत्रों में किसान जल-निधि से संबंधित परिस्थितियों का सामना करते हैं। प्रतिदिन ही उन्हें सिंचाई संबंधी योजनाएं करनी होती है, क्योंकि वर्षा अनिश्चित होती है एवं पूर्वमेव घटे हुए भूजल स्तर की स्थितियों में जल का अपव्यय करना उचित नहीं। यदि किसानों को पूर्व में ही यह ज्ञात हो सके कि आने वाले सप्ताहों में उन्हें कितना वर्षाजल प्राप्त होगा, तो वे सिंचाई का प्रभावी प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे उपज की वृद्धि के साथ-साथ भूजल संरक्षण भी संभव होगा।
उक्त समस्या के निवारण हेतु सिविल अभियांत्रिकी विभाग एवं जलवायु अध्ययन केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्स्थान (आईआईटी) मुंबई, तथा भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे (आईआईटीएम, पुणे) के शोधकर्ताओं ने एक विधि विकसित की है। अपने नव्यसा अध्ययन में उन्होंने आईआईटीएम पुणे से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के विस्तारित अवधि के आंकड़ों (1 से 3 सप्ताह आगे तक), आईआईटी मुंबई द्वारा संसाधित उपग्रह से प्राप्त मिट्टी की आर्द्रता का डेटा (सॉइल मॉइस्चर डेटा) तथा एक कंप्यूटर मॉडल का संयोजन कर, आगामी तीन सप्ताह तक सिंचाई जल की आवश्यक मात्रा का पूर्वानुमान किया। इस प्रणाली का जनपद एवं उप-जनपद स्तर पर प्रयोग किया गया।
महाराष्ट्र के नाशिक में किये गए प्रायोगिक अध्ययन (पायलट स्टडी) में शोधकर्ताओं ने पाया कि अंगूर की कृषि करने वाले कुछ समृद्ध किसान, मिट्टी की शुष्कता के परीक्षण हेतु स्थानीय मिट्टी आर्द्रता संवेदक (सॉइल मॉइस्चर सेंसर) का प्रयोग करते हैं। यदि संवेदक मिट्टी में शुष्कता को इंगित करता है तो किसान अंगूर के खेत की सिंचाई कर देते हैं। अब यदि अंगूर के इस सिंचित खेत में वर्षा हो जाती है तो सिंचित जल का अपव्यय (वेस्टेज) होता है। पहले से ही घटे हुए भूजल स्तर वाले इन क्षेत्रों में जल अपव्यय को रोकने हेतु, अध्ययनकर्ता मौसम पूर्वानुमान की जानकारी को जोड़े जाने का प्रस्ताव देते हैं ताकि सिंचाई संबंधी सही निर्णय लिया जा सके।
“नाशिक में किये गए प्रायोगिक अध्ययन में हमने मिट्टी आर्द्रता डेटा के साथ स्थानीय मौसम पूर्वानुमान को भी सम्मिलित किया एवं किसानों को दिखाया कि इस प्रकार से 30% तक भूजल संरक्षण किया जा सकता है। प्रारंभिक रूप से हमने केवल अल्पावधि अर्थात एक सप्ताह आगे तक का अनुमान दिया,” आईआईटी मुंबई के प्राध्यापक सुबिमल घोष ने बताया।
इस अल्पावधि के पूर्वानुमान के साथ शोधकर्ताओं ने मौसम के पूर्वानुमान एवं मिट्टी की आर्द्रता संबंधित डेटा को एक कंप्यूटर मॉडल में संप्रेषित किया। यह मॉडल वर्षा की संभावित मात्रा, मिट्टी की जल धारिता (वाटर कैपेसिटी) एवं प्रत्येक उपज के लिए आवश्यक जल की मात्रा का परीक्षण करता है। कब एवं कितना पानी किस उपज के लिए आवश्यक है, यह विवरण देने में कंप्यूटर मॉडल सक्षम है। यदि मॉडल के अनुमान के अनुसार आगामी दिनों में वर्षा नहीं होने वाली है, तो उपज की सिंचाई का संकेत दिया जाता है। इसके विपरीत यदि मॉडल वर्षा होने का अनुमान करता है, जो कि मिट्टी की आर्द्रता में वृद्धि कर सकती है, तो मॉडल उपज की सिंचाई का कार्यक्रम स्थगित करने का संकेत देता है। उनकी खोज ने दर्शाया कि उपज में बिना किसी कमी के 10 से 30 % कम पानी के साथ भी अंगूर की कृषि की जा सकती है। यह पद्धति उपज की अतिरेक सिंचाई को रोकती है, अतः जल संरक्षण में सहायक है।
शोधदल ने अपनी इस पद्धति को पश्चिम बंगाल के एक सूखा प्रवण जनपद, बाँकुरा के 12 उपजनपदों में कार्यान्वित किया। उन्होंने अनाज, तिलहन एवं भुगतान उपजों (कैश क्रॉप) को विचार में लेते हुए मक्का, गेहूं, सूरजमुखी, मूंगफली एवं गन्ना जैसी पांच प्रमुख उपजों पर ध्यान केंद्रित किया। व्यापक रूप से रोपी जाने वाली इन उपजों में विकास के विविध विन्यास (पैटर्न) एवं जल की भिन्न-भिन्न आवश्यकताएं होती हैं। प्रत्येक उपज में मिट्टी की सतह के नीचे की गहराई भिन्न-भिन्न होती है, जहाँ इसके मूलखण्ड पानी एवं अन्य पोषण ग्रहण करते हैं। मूलखण्ड के इन गहराईयों तक मिट्टी में पर्याप्त आर्द्रता होना आवश्यक होता है। पौधों को पर्याप्त जल नहीं मिलने पर वे जल-तनाव (वाटर स्ट्रेस) का संवेदन करते हैं। तब जल संवर्धन हेतु वे स्टोमेटा नामक अपने पत्तों पर स्थित सूक्ष्म छिद्रों को बंद कर लेते हैं, जो कि वायु के आदान-प्रदान करने के लिए होते हैं।
मूलखण्ड की गहराई, मिट्टी की संरचना, सरंध्रता, जल धारिता, जल चालकता (वाटर कंडक्टिविटी) एवं स्टोमेटा के बंद होने की प्रक्रिया जैसे मिट्टी आर्द्रता डेटा प्राप्त करने हेतु शोधकर्ताओं ने ग्लोबल सॉइल मानचित्र (वैश्विक मृदा का मानचित्र) एवं एकीकृत सेटेलाइट तथा क्षेत्रीय डेटा का उपयोग किया। वैज्ञानिकों ने जल उपभोग, मासिक वर्षा, मूलखण्ड की गहराई एवं आवश्यक सिंचाई जल से संबंधित डेटा संग्रह हेतु फ़ूड एन्ड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) रिसोर्स, भारत मौसम विज्ञान विभाग के डेटाबेस एवं आईआईटीएम पुणे की सहायता ली।
प्रा. घोष ने मॉडल के बारे में बताते हुए कहा, “हमारा कंप्यूटर मॉडल पौधों के द्वारा मिट्टी से पानी ग्रहण किये जाने की प्राकृतिक प्रक्रिया को दर्शाता है, साथ ही जल-तनाव अर्थात पानी की कमी के समय पौधे की अनुकूलन क्षमता एवं सिंचाई या वर्षा के उपरांत जल संतुलन के समय उनकी प्रतिक्रिया को भी दर्शाता है।”
इस नवीन पद्धति ने जल प्रबंधन के लिए वास्तविक समय में एक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया। शोधकर्ताओं ने उपज के समस्त प्रकारों पर कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करते हुए आगामी तीन सप्ताहों के लिए मिट्टी, मौसम एवं उपज आवश्यकताओं तथा मौसम के प्रत्यक्ष आंकड़ों के साथ इस पद्धति की पुष्टि की। इस योजना के कार्यान्वयन से इन 12 उप-जनपदों में पारंपरिक सिंचाई विधियों की तुलना में 10 से 30% तक जल का संरक्षण किया जा सकता है।
“हम अत्यधिक उपज विशिष्ट मॉडल नहीं चाहते थे अतः हमने अधिक सामान्यीकृत समीकरण (जनरलाइज्ड इक्वेशन) विकसित किए हैं। हमने एक सरलतम पारिस्थितिकी जलविज्ञान (इकोहाइड्रोलॉजिकल) मॉडल का उपयोग किया है, जिसमें मौसम पूर्वानुमान एवं मिट्टी की आर्द्रता से संबंधित आंकड़ों का उपयोग किया गया है। मॉडल को क्षेत्र एवं उपज के आधार पर समायोजित किया जा सकता है,” प्रा. घोष ने आगे बताया।
विस्तारित अवधि का मौसम पूर्वानुमान, जनपद स्तर की जल आवश्यकताओं की सूचना देकर जल प्रबंधन में सहायता करता है। विभिन्न प्रकार की उपजों एवं मिट्टी के प्रकारों पर आधारित मॉडल का उपयोग करके जल का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा सकता है।
“इस उपयोगी पद्धति को अन्य जनपदों तक प्रसारित करने हेतु, हमें किसानों को इस मॉडल के लाभों के संबंध में विश्वास दिलाना होगा। इस संबंध में हम, ग्रामों में कुछ संवेदक (सेंसर) स्थापित करने तथा परामर्श केंद्र निर्मित करने हेतु किसानों से वार्ता करने की योजना बना रहे हैं,” प्रा. घोष ने कहा।
अध्ययन दर्शाता है कि मौसम पूर्वानुमान, दूरस्थ संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं संगणक प्रतिरूप-विधान (कंप्यूटर सिमुलेशन) को एक साथ जोड़ देने पर, यह सिंचाई प्रबंधन में एवं भूमिगत जल पर निर्भरता को कम करने में किसानों एवं जल प्रबंधकों की प्रभावी रूप से सहायता कर सकता है।
परियोजना वित्तीय सहायता: यह कार्य पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यावरण विभाग, डीएसटी-स्वर्णजयंती फेलोशिप योजना, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स, लार्ज इनीशिएटिव्स एंड कोऑर्डिनेटेड ऐक्शन एनेबलर (SPLICE), क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम (CCP) के एक भाग तथा ऑरेकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के द्वारा वित्त पोषित किया गया है।