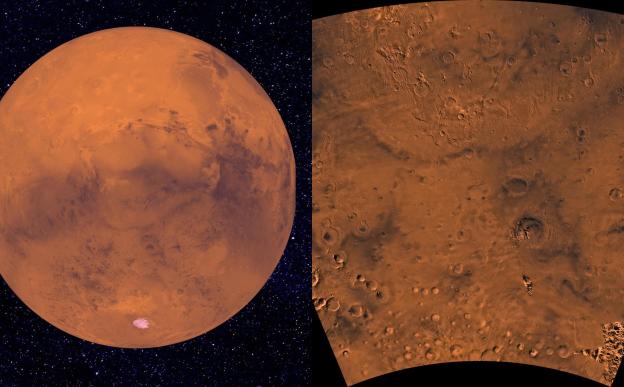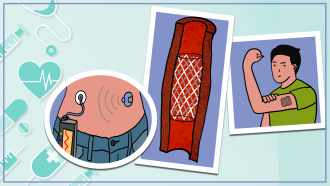विज्ञान जगत की कथाओं (Sci-fi) के समानांतर स्थित ब्रह्मांड का कोई पात्र, यदि उपलब्ध विकल्पों के स्थान पर कोई अन्य विकल्प चुने तो कथा में असीमित संभावनाएँ प्राप्त हो सकती हैं। गंतव्य प्राप्ति हेतु सामान्यतः उपयोग की जाने वाली बस के स्थान पर यदि हम रेलयात्रा का चयन करते हैं तो विभिन्न नवीनतम अनुभव प्राप्त होते हैं, किंतु दोनों यात्राओं के माध्यम से हम अंतत: एक ही गंतव्य स्थान पर पहुँचते हैं। संभवतः प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हो। उदाहरण स्वरूप भोज्य पदार्थ में परिवर्तन होने पर डार्विन की फिंच चिड़िया की चोंच पृथक रूप से अनुकूलित हुई। खाद्य स्रोतों में कितनी भिन्नता होनी चाहिये ताकि प्रजातियों को विकासक्रम के विभिन्न परिणामों में अनुकूलित किया जा सके? क्या खाद्य पदार्थों में किया गया सूक्ष्म सा परिवर्तन इस प्रकार के अनुकूलन में परिणामित हो सकता है? एवं क्या किसी प्रकार से इन प्रजातियों के भविष्य का पूर्वानुमान किया जा सकता है? विकासक्रम संबंधी जीवविज्ञान के इन आधारभूत प्रश्नों से वैज्ञानिक दशकों से जूझ रहे हैं ।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई (आईआईटी मुंबई) के रसायन अभियांत्रिकी विभाग के शोधकर्ताओं ने सूक्ष्मजीवों के स्तर पर होने वाली इस प्रक्रिया के मर्म की व्याख्या की है। अपने दो नव्यसा अध्ययनों में शोधदल ने दो प्रकार के सूक्ष्जीवियों (माइक्रोब्स) का उपयोग किया। इनमें से एक चिर-परिचित बैक्टीरियम Escherichia coli या ई. कोलाय है, जो एक सामान्य आंत्र जीवाणु है, तथा दूसरा यूकार्योटिक यीस्ट Saccharomyces cerevisiae है, जो बेकिंग में उपयोग होने वाला पदार्थ है। वैज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयत्न किया कि भोजन के रूप में एक ही प्रकार की शर्करा को भिन्न-भिन्न प्रकार से दिए जाने पर सूक्ष्जीवियों के उद्विकास (एवोल्यूशन) की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होता है।
किसी जीवतत्व के स्वरूप में समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले परिवर्तन को उद्विकास (इवोल्यूशन) कहा जाता है। यह अपने आप में प्रथम अध्ययन है जो दर्शाता है कि अन्यथा-एकसमान वातावरण में केवल सूक्ष्म सा अंतर भी विकासक्रम में भिन्नता उत्पन्न कर सकता है। अपने प्रयोग के लिए शोधकर्ताओं ने सूक्ष्जीवियों (माइक्रोब्स) के एक समूह को ग्लूकोज़ एवं दुग्ध उत्पादों में पाए जाने वाले गैलेक्टोज़ शर्कराओं का मिश्रण दिया। जबकि दूसरे समूह को उसी ग्लूकोज़ एवं गैलेक्टोज़ से निर्मित जटिल शर्करा, मेलिबीओस या लेक्टोज़ दी गई।
वास्तव में इन सूक्ष्जीवियों को बराबर मात्रा में ग्लूकोज़ एवं गैलेक्टोज़ दिया गया किंतु इनके स्वरूपों में भिन्नता थी। शर्कराओं के समान होने किन्तु उनके स्वरूपों में सूक्ष्म सा अंतर होने के कारण इस खाद्य स्रोत को ‘समान’ माना जाता है। यह अंतर वैसा ही है जैसा कि डोसा एवं दाल-चावल में है, यद्यपि घटक समान ही रहते हैं, किंतु स्वरूप भिन्न होते हैं। शोधकर्ताओं ने तीन प्रकार की शर्कराओं की उपस्थिति में इन सूक्ष्मजीवियों की सैकड़ो पीढ़ियों को विकसित होने दिया, जिससे इस सूक्ष्मजैविक संसार में उद्विकास की प्रक्रिया सुगम हो सकी।
“हमने रासायनिक रूप से परस्पर समान शर्कराओं का उपयोग किया। हमारा उद्देश्य यह अवलोकन करना था कि क्या इन सूक्ष्मजीवियों पर भोजन प्रस्तुति की इस प्रक्रिया का कुछ प्रभाव होता है,” अध्ययन प्रमुख आईआईटी मुंबई के प्रा. सुप्रीत सैनी का कहना है।
पीढ़ियाँ व्यतीत होने के उपरांत, सूक्ष्म से अंतर के साथ प्रस्तुत किया गया यह भोजन इन सूक्ष्मजीवियों को उद्विकास के पथ पर विभक्त होने का माध्यम बनता है। तीन सौ पीढ़ियों के उपरांत जीवाणुओं के एक समूह में उच्च वृद्धि दर देखी गई जबकि दूसरे समूह में जैविक भार (कुल मात्रा) की अधिकता दिखाई दी। इस प्रकार यह विभाजन, वृद्धि के दो विशिष्ट प्रकारों को दर्शाता है। ऐसे ही विभक्त परिणाम यीस्ट समूह में भी देखे गए। शर्करा संघटन (कम्पोजीशन) के आधार पर सूक्ष्जीवियों का प्रत्येक समूह दो ऐसे विकासक्रमों में अनुकूलित (अडाप्ट) होता है जिनका अनुमान लगा पाना संभव नहीं। आनुवांशिक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इस अनुकूलन का कारण विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) थे।
“हमें इतने सूक्ष्म से अंतर (भोज्य पदार्थ/ पोषक तत्वों में) के साथ पूर्णतः पृथक अनुकूलन पथों के उत्पन्न होने की अपेक्षा नहीं थी। अध्ययन के परिणाम इंगित करते हैं कि दिए गए पोषक तत्वों के प्रति कोशिका की प्रतिक्रिया यह निर्धारित कर सकती है कि कौन सा उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) लाभदायक होगा एवं उद्विकास (इवोल्यूशन) की प्रक्रिया किस पथ पर अग्रसर होगी,” पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ता नीतिका अहलावत ने बताया, जो दोनों अध्ययनों की एक लेखिका हैं।
भोजन के एक विशिष्ट स्रोत के माध्यम से होने वाला सूक्ष्मजीवों का अनुकूलन, किसी नए वातावरण में उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। दिए गए वातावरण में यह प्रभाव ‘प्लियोट्रोपिक प्रतिक्रिया’ या अनुकूलन के अतिरिक्त प्रभाव के रूप में जाना जाता है। जब शोधकर्ताओं ने ई-कोलाय एवं यीस्ट दोनों के उद्विकसित समूहों का नए शर्करा स्रोतों में स्थानांतरण किया तो उनका विकास आश्चर्यजनक रूप से एक अनुमानित विन्यास क्रम (प्रेडिक्टेबल पैटर्न) में था। इस प्रकार जिस वातावरण में ये सूक्ष्मजीवी उत्पन्न किये गए थे वहाँ उनके समूहों के प्रदर्शन का अनुमान लगा पाना हमारे लिए असंभव था, जबकि उद्विकास के अतिरिक्त प्रभाव का अनुमान सफलतापूर्वक लगाया जा सका!
“पुनश्च, उद्विकास की प्रक्रिया लचीली अर्थात विभक्तिग्राही होने के साथ साथ सीमाबद्ध भी है। समरूप वातावरण में परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सका, जो उद्विकास की प्रक्रिया के लचीले होने की संभावना व्यक्त करता है। यद्यपि नए वातावरण में इस उद्विकास का प्लियोट्रोपिक नामक अतिरिक्त प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत था। एक विकसित समूह के द्वारा किसी अन्य वातावरण में किये जाने वाले प्रदर्शन का पूर्वानुमान, उनके पूर्वजों के व्यवहार के आधार पर किया जा सकता है,” पूर्व शोध छात्र पवित्रा वेंकटरमन जो ई-कोलाय अध्ययन की एक लेखिका भी हैं, कहती हैं।
इस खोज का विस्तार बड़े स्तर के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। संसाधन संयोजनों में संशोधन करके सूक्ष्मजीवियों में लाभकारी गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है। परिणामी उन्नत विकास दर एवं श्रेष्ठ उपापचायज (उपापचय प्रक्रिया से प्राप्त उपयोगी पदार्थ या मेटाबोलाइट) का उपयोग व्यावसायिक अनुप्रयोगों जैसे खाद्य एवं पेय पदार्थों, औषधि निर्माण एवं जैव-ईंधन उद्योगों में किया जा सकता है।
“आवश्यक संसाधनों के साथ हम रोग कारक जीवाणुओं (पैथोजन्स) के उद्विकास पथ को अवरुद्ध कर सकने की कल्पना अब कर सकते हैं ताकि इनके ऐंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास को कठिन बनाया जा सके। अभी यह खोज अपनी आरंभिक अवस्था में है, किंतु संभावना उत्साहजनक है,” प्रा. सैनी बताते हैं।
बहुत से कथानकों से युक्त एक काल्पनिक कथा के समान, उद्विकास असीमित विविधताएं उत्पन्न कर सकता है। दोनों में समानताएं हैं - समान आरंभ, एक पहेली (ट्विस्ट), एवं विभिन्न प्रकार के अनुभव जो कुछ अव्यक्त नियमों के आधार पर एक पूर्वानुमानित अंत की ओर ले जाते हैं। खोज के परिणाम बताते हैं कि हम परिणामों को न केवल देख सकते हैं अपितु इन अव्यक्त नियमों को सीखकर इनकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं !