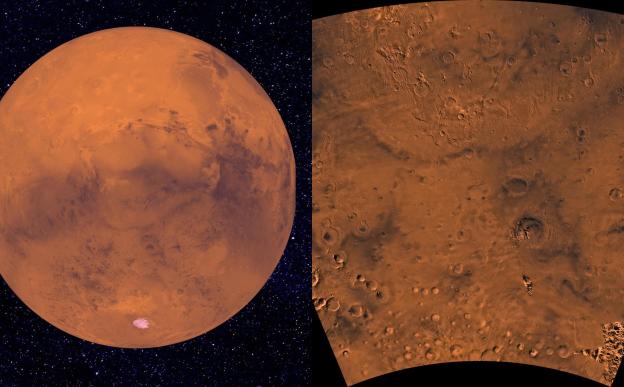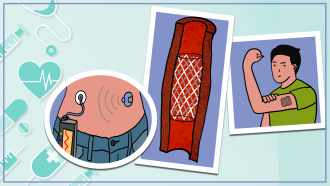भारत एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है एवं अपने महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश के पास पर्याप्त समय नहीं है। 50% से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन की क्षमता पहले ही स्थापित हो चुकी है, और विद्युत् मंत्रालय द्वारा ऊर्जा उपभोग का 43.33% भाग नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने का जनादेश भी जारी है। इससे देश एक महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन की कगार पर है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency; IRENA) के अनुसार, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वैश्विक स्तर पर चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता तीसरे स्थान पर है। यद्यपि, एक अरब से अधिक लोगों के देश के लिए, बिना आर्थिक भार बढ़ाए या विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाए, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना एक जटिल चुनौती होगी।
इस दिशा में कार्य करते हुए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई (आईआईटी मुंबई), नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस), और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी दिल्ली) के शोधकर्ताओं ने भारत के लिए शाश्वत विद्युत व्यवस्था हेतु एक व्यापक रोडमैप विकसित किया है। उनका नया कम्प्यूटेशनल मॉडल नवीकरणीय ऊर्जा जनादेश (रिन्यूएबल एनर्जी मैंडेट) को पूरा करने के लिए स्थिति-आधारित लागत का अनुमान प्रदान करता है और विद्युत संयंत्रों (पॉवर प्लांट्स) की योजना और संचालन के अनुकूलन में मार्गदर्शन कर सकता है।
आईआईटी मुंबई के प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ फेलो) निखिल तेजेश वेंकटरमना कहते हैं, “हमारा अध्ययन भारत की तेजी से विकसित हो रही विद्युत प्रणाली को मॉडल करने के लिए एक नया, उच्च-रिज़ॉल्यूशन दृष्टिकोण लाता है, विशेषतः जब देश शीघ्रता से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने की व्यावहारिक चुनौती का सामना कर रहा है।” निखिलने प्रा. वेंकटसैलनाथन रामादेसिगन (आईआईटी मुंबई), प्रा. तेजल कानिटकर (एनआईएएस), और प्रा. रंगन बनर्जी (आईआईटी दिल्ली) के मार्गदर्शन में यह अध्ययन किया है।
हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं और अंतर-राज्य विद्युत प्रवाह को पूरा करने के मार्ग को सफलतापूर्वक मॉडल करने के लिए, दो प्राथमिक पहलुओं पर विचार करना होगा : उपलब्ध तथा विकसित हो रही आधारभूत संरचनाएँ (इंफ्रास्टक्चर), एवं किसी प्रणाली की निवेश और परिचालन लागत। शोधकर्ताओं ने एक ‘क्षमता विस्तार’ (कपैसिटी एक्सपैंशन) और ‘आर्थिक प्रेषण’ (इकोनॉमिक डिस्पैच) पर आधारित कम्प्यूटेशनल मॉडल विकसित किया, जिसने इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखा। उनके मॉडल का क्षमता विस्तार भाग नवीकरणीय ऊर्जा जनादेश की पूर्ति करने के साथ ही विद्युत की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए नए विद्युत संयंत्रों और बैटरी भंडारण (स्टोरेज) के सबसे कम लागत वाले इष्टतम संयोजन और मात्रा का निर्धारण करता है। मॉडल का आर्थिक प्रेषण भाग अत्यधिक बारीकी से कार्य करता है, एवं प्रत्येक 15 मिनट में यह निश्चित करता है कि कौन से विद्युत संयंत्रों को चलाना चाहिए और वे कितनी ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। मॉडल का यह भाग विद्युत संयंत्रों को सबसे कम संभाव्य लागत पर मांग को पूरा करने के लिए संचालित कर सकता है, साथ ही उनकी परिचालन सीमाओं को भी ध्यान में लेता है। मॉडल के इन दोनों भागों के एकीकरण के माध्यम से नई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के बारे में होने वाले निर्णय, सीधे इस बात से सूचित होते हैं कि उस आधारभूत संरचना को वास्तविक समय में कितनी कुशलता से संचालित किया जा सकता है।
निखिल बताते हैं, “हमारे मॉडल में क्षमता विस्तार और आर्थिक प्रेषण को एकीकृत कर ऐसा अनुकूलन ढाँचा (ऑप्टिमाइज़ेशन फ्रेमवर्क) विकसित किया गया है, जो विद्युत प्रणाली का सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण एवं सर्वोत्तम संचालन सुनिश्चित करता है। यह जिएएमएस (जनरल अलजेब्रिक मॉडलिंग सिस्टम) नामक एक गणितीय प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके बनाया गया है।”
इस अध्ययन में भारत के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के नौ राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। निखिल के अनुसार, इन राज्यों को इसलिए चुना गया क्योंकि “ये क्षेत्र सामूहिक रूप से देश की आधी से अधिक विद्युत् की मांग (~56%, वित्तीय वर्ष 2023-24 में ~905 टेरावॉटघंटे), देश की 42% जनसंख्या (2023 में 59.2 करोड़), तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 59% के भागीदार हैं। यह पहलु हमारे अध्ययन को भारत के समग्र ऊर्जा परिदृश्य का उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।” उनका मॉडल 2022-23 के आधारभूत वर्ष से चल कर 2030 के लक्ष्य वर्ष पर केंद्रित होता है।
मॉडल की रचना हेतु, शोधकर्ताओं ने 15 मिनट के बारीक़ समय-अंतराल में राज्य और यूनिट स्तर की विद्युत की मांग और उत्पादन का डेटा एकत्र किया।
निखिल कहते हैं, “हमने ग्रिड-इंडिया (पूर्व में पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू)को औपचारिक रूप देकर पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (WRLDC) और राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (NLDC) के सहयोग के माध्यम से यह विस्तृत डेटा प्राप्त किया।”
डेटा में इस स्तर की बारीकी (ग्रेन्यूलैरिटी) महत्वपूर्ण है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अस्थिर तथा मौसम पर निर्भर होते हैं। इनके तीव्र परिवर्तनों को ट्रैक करके, मॉडल यह सटीक रूप से दर्शा सकता है कि सौर और पवन ऊर्जा कैसे उतार-चढ़ाव करती है, थर्मल प्लांट कैसे काम करते हैं, और कितने लचीले संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे बैटरी और ट्रांसमिशन लाइनें।
इस अध्ययन से पता चला कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का समाधान राज्यों में समन्वित योजना और ऊर्जा भंडारण के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण में निहित है। शोधकर्ताओं ने पाया कि राज्यों और क्षेत्रों के मध्य विद्युत् को मुक्त रूप से प्रवाहित कर, भारत और अधिक मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करते हुए समग्र प्रणाली लागत को महत्वपूर्ण मात्रा में कम कर सकता है। विश्लेषण से पता चला है कि स्वतंत्र तथा राज्य-वार प्रेषण के स्थान पर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में समन्वित संचालन में परिवर्तन करने से कुल स्थापित क्षमता की आवश्यकता 314 GW से घटकर 288 GW हो जाती है। यह कमी 20% रिन्यूएबल पर्चेस ऑब्लिगेशन (आरपीओ), अर्थात नवीकरणीय खरीद दायित्व पर आधारित थी। आरपीओ वितरण कंपनियों एवं संस्थाओं जैसे बड़े उपभोक्ताओं को उनके कुल विद्युत् की खपत का एक न्यूनतम प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से खरीदने के लिए बाध्य करने वाला एक सरकारी जनादेश है ।
राज्यों के मध्य यह समन्वय लागत में पर्याप्त बचत संभव करता है, जिससे लक्ष्य वर्ष २०३० तक समग्र प्रणाली लागत में लगभग ₹12 लाख करोड़ (लगभग 14 अरब अमेरिकी डॉलर) का घटाव होता है। विविध विद्युत् मांगों और नवीकरणीय संसाधनों को एकत्रित करने की क्षमता से यह उल्लेखनीय दक्षता आती है। उदाहरण के लिए, विभिन्न राज्यों में अतिउच्च विद्युत् उपभोग के समय भिन्न-भिन्न होते हैं. राज्यों को जोड़कर, समग्र ग्रिड में अतिउच्च और अतिनिम्न भार का अनुभव कम होकर संतुलन बना रह सकता है। संसाधन से समृद्ध राज्य, जैसे पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु या सौर ऊर्जा के लिए गुजरात, अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और इस ऊर्जा को उन राज्यों को भेज सकते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इससे उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा का अच्छा उपयोग हो सकता है और प्रत्येक राज्य को महंगे अतिरिक्त (बैकअप) विद्युत् संयंत्रों का निर्माण करने की आवश्यकता कम हो सकती है।
निखिल कहते हैं, “क्षेत्रीय एकीकरण से होने वाले लाभ आश्चर्यजनक स्तर पर बड़े थे। अंतरक्षेत्रीय एवं क्षेत्र के अंदर के समन्वय से 10-15% प्रणाली लागत की बचत हुई और स्थापित क्षमता 20-30 GW से घटी। ये परिणाम सहकारी योजना और संचरण-सक्षम लचीलेपन के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करते हैं।”
अध्ययन में नवीकरणीय ऊर्जा के वृद्धि हेतु आवश्यक एक महत्वपूर्ण संतुलन पर भी प्रकाश डाला गया है : कोयला-आधारित उत्पादन और बैटरी भंडारण के बीच संतुलन (ट्रेड-ऑफ़)। यदि नए कोयला और जलविद्युत् क्षमता को केवल उन परियोजनाओं तक सीमित कर दिया जाए जो पहले से ही निर्माणाधीन हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा को उच्च प्रतिशत में एकीकृत करने के लिए इस उत्पन्न ऊर्जा के भंडारण के लिए बड़ी मात्रा में बैटरी स्टोरेज की आवश्यकता होगी। मॉडल का अनुमान है कि, लगभग 29-41% नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए, बैटरी स्टोरेज को पश्चिमी क्षेत्र में 125 GW तक और दक्षिणी क्षेत्र में 70 GW तक वृद्धि की आवश्यकता होगी।
तकनीकी रूप से संभव होने के उपरांत भी, वर्तमान लागतों को देखते हुए 2030 तक बैटरी का इस तरह का तीव्र विस्तार भारत के लिए सबसे अधिक व्यावहारिक तथा किफायती समाधान नहीं हो सकता है।
निखिल के अनुसार, “प्रश्न यह नहीं है कि 2030 से पहले बैटरी उपलब्धि को शीघ्रता से कैसे बढ़ाया जाए। किन्तु प्रश्न यह है कि कोयले के (ऊर्जा उपयोग) को चरण-वार बंद करने के साथ-साथ, मध्यम से दीर्घ अवधि में बैटरी भंडारण क्षमता में क्रमिक और लागत-प्रभावी वृद्धि कैसे की जाए।”
इस कार्य में शोधकर्ताओं ने एक व्यावहारिक मार्ग का प्रस्ताव दिया है।प्रस्तावित मार्गमें पुराने एवं कम कुशल कोयला-आधारित संयंत्रों को युक्तिपूर्ण एवं क्रमिक रूप से चरण-वार बंद करना, रणनीतिक स्थानों में बैटरी भंडारण का वृद्धिशील विकास, तथा देशांतर्गत विनिर्माण एवं वैश्विक प्रगति के माध्यम से बैटरी लागत को कम करने के लिए निरंतर प्रयास सम्मिलित हैं।
भारत के सुधारित नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग के जनादेश पर ध्यान केंद्रित करके और अंतरक्षेत्रीय संचरण को स्पष्ट रूप से मॉडल करके, यह अध्ययन नीति निर्माताओं को अधिक व्यावहारिक और तत्काल अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। राष्ट्र की वर्तमान आर्थिक मर्यादाओं पर भी मॉडल प्रकाश डालता है, एवं नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण विस्तार में पर्याप्त लागत में कमी और नीति समर्थन की आवश्यकता का प्रस्ताव देता है। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के मध्य के संतुलन और क्षेत्रीय सहयोग के लाभों को व्यवस्थित रूप से मॉडल करके, यह अध्ययन भारत के लिए अपने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा दिखाता है।
निखिल निष्कर्ष देते हैं, “हमारा विस्तृत और नीति-प्रासंगिक दृष्टिकोण भारत के शाश्वत ऊर्जा भविष्य की योजना के लिए एक शक्तिशाली साधन प्रदान करता है। अतः इस बात की अंतर्दृष्टि मिलती है कि कैसे समन्वित क्षमता विस्तार, लक्षित भंडारण परिनियोजन, और उन्नत संचरण सुविधाएं सामूहिक रूप से एक लागत-प्रभावी, विश्वसनीय, और पर्यावरणीय रूप से दृढ़ विद्युत् प्रणाली को प्रोत्साहन दे सकते हैं।”